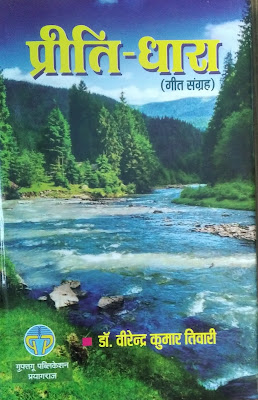समाजिक सौहार्द में कविता का बहुत बड़ा रोल है : आईएएस डॉ. अखिलेश मिश्र
 |
| डॉ. अखिलेश मिश्र |
वरिष्ठ आईएएस डॉ. अखिलेश मिश्र वर्तमान के जाने-माने साहित्यकार हैं। मुशायरों में शिरकत करने के लिए इन्हें पूरे देश के अलावा दुबई, श्रीलंका, सिंगापुर और थाईलैंड समेत कई देशों में आमंत्रित किया जा चुका है। इनकी पुस्तक ‘यूं ही’ काफी लोकप्रिय है, ऑनलाइन बेस्ट सेलर में की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले डॉ. अखिलेश मिश्र ने बी.एच.यू. से एम.एस-सी. करने के साथ ही पी.एच-डी. किया है। बिहार सरकार के कृषि विभाग में अल्पकालिक नौकरी से शुरुआत करने के बाद आप रजिस्ट्रार-लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ; सीईओ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उ.प्र.; विशेष सचिव, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उ.प्र. सरकार रहने के साथ-साथ कई जिलों में जिलाधिकारी रहे चुके हैं। उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में विशेष सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, उ. प्र. के महत्वपूर्ण पद पर लखनऊ में कार्यरत हैं। उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाले, कुशल प्रशासक के रूप में चुनाव प्रबंधन एवं दंगे रोकने में दक्ष, हरफन मौला आदरणीय डॉ. अखिलेश मिश्रा जी पर्यावरण प्रेमी प्रशासनिक अधिकारी के साथ-साथ लोकप्रिय कवि एवं रामकथा वाचक भी हैं। डॉ. अखिलेश मिश्रा जी का जन्म 27 जून 1965 को हुआ है। आपका गृह नगर जौनपुर, उत्तर प्रदेश है। आपने एम.एससी. एवं पीएच.डी. की उपाधि, बी. एच. यू., वाराणसी से प्राप्त की। जितनी कुशलतापूर्वक वो प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं उतनी ही कुशलता से वो सटीक एवं संवेदनशील काव्य का सृजन भी करते हैं। प्रशासनिक पद पर रहने के कारण, देश और समाज की परिस्थितियों पर खुलकर न बोल पाने की मजबूरियों के कारण, उनके संवेदनशील हृदय में उपजता उनका आक्रोश/घुटन/ वेदना, संवेदनशील कविताओं/ शायरी के रूप में निरंतर प्रस्फुटित होता रहता है।अशोक श्रीवास्तव ‘कुमुद’ ने इनसे मुलाकात करके विस्तृत बातचीत की है। प्रस्तुत इस बातचीत के प्रमुख भाग।
सवाल: आपने समय-समय पर विभिन्न विभागों में कार्य किया है। किस विभाग में कार्य करते हुए आपको सबसे अधिक रुचिकर लगा ?
जवाब: आप का प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, और यदि ये पूछा जाय कि कौन सा रूप मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तो इसका उत्तर, समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। एक समय पर सारे रूप पसंद हो या सारी चीजें एक समय में की जा सकें, ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। माहौल के अनुसार, हम लोगों की लिमिटेशन होती है। हम सब बहुत ज्यादा सरकार के पक्ष या विपक्ष में अथवा राजनीतिक परिस्थितियों या धार्मिक पहलू के अनुसार, सार्वजनिक रूप से अपने आपको पेश नहीं कर सकते। विभिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार सब कुछ, हर जगह नहीं चल पाता है। अपनी लिमिटेशन/लिब्रिकेशन में, जिस चीज को जितना हम जी लेते हैं, उस समय वही अच्छा लगता है। इसका एक जवाब नहीं हो सकता है। समय काल और परिस्थिति के अनुसार कोई भी चीज कहीं ज्यादा अच्छी लगती है तो कहीं कम अच्छी।
सवाल: रिटायर्मेंट के बाद आप कौन सा रूप अपनाना चाहेंगे ?
जवाब: इतना पहले से प्लानिंग करके मैं जीता नहीं हूं। हम लोग दिन-प्रतिदिन के आधार पर निर्णय करते हैं। बहुत लम्बी प्लानिंग कभी जिंदगी में, नहीं की है। न पुराने की कोई चिंता रहती है न भविष्य की कोई फिक्र होती है।
सवाल: प्रशासनिक सेवा में रहते हुए, कविता या शायरी की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ, शुरूआत कैसे हुई?
जवाब: प्रशासनिक सेवा के शुरूआती दौर में, नैतिक-सैद्धांतिक भावनाएं, हर प्रशासनिक अधिकारी के दिलो-दिमाग में भरी होती हैं। वह अपने आप को एक राजा की तरह देखता, सोचता है। नैतिक रूप से ईमानदार, न्यायप्रिय व्यक्ति होता है, परंतु धीरे-धीरे परिस्थितियां, व्यक्ति पर हावी होने लगती हैं। तब अलग-अलग स्तर पर डायलूशन होने लगता है। कभी हम नैतिक रूप से अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, कभी अन्य रूप में कमज़ोर पाते हैं, कभी व्यवस्था हमें कमज़ोर कर देती है। तो जब इन चीज़ों को, हम देखते हैं और जहां पर, हम अपने आपको कमज़ोर पाते हैं तो वो कसमसाहट या छटपटाहट कविता के रूप में उभरकर आती है। खुशियां सामान्यतः कविता नहीं पैदा करती हैं, सामान्यतः दुख, कविता पैदा करती है। चिंता या गम पैदा करती है जो आप नहीं कर पाए रहे हैं उसको कर लेने की इच्छा, वो आपके अंदर कविता पैदा करती है। व्यक्तिगत रूप से अगर कविता की बात करें तो समारोहों में चीफ गेस्ट बनते-बनते मैंने कविता सीखी। शुरूआती दौर में, मैं जब डिप्टी कलेक्टर था तो मेरी कलेक्टर एक महिला थी और सामान्यतः ऐसे कार्यक्रमों में वह नहीं जाया करती थी, तो सारे इलाके में इस दायित्व का निर्वहन मुझे ही करना पड़ता था। सामान्यतः वहां मैं अपने उद्बोधन में दूसरों की रचनाएं ही सुनाता था जैसे बच्चन जी की मधुशाला, वगैरह। जब-जब मैं मधुशाला सुनाता था तो अक्सर, युवा लोग मेरे फैन हो जाते थे। परंतु एक बार मंच पर डॉ हरि ओम पंवार जी ने मुझसे मंच पर ही कहा कि लगता है कि मधुशाला तुमने ही लिखी है, और आगे से मंच पर मेरे सामने आना तो अपनी लिखी कविता लेकर आना, नहीं तो मेरे सामने मंच पर मत आना। मेरठ का माहौल था मेरे सारे फैन थे, बड़े-बड़े कवि थे, मुझे बहुत खराब लगा कि कोई सार्वजनिक रूप से ऐसे हड़का दे। मैंने फिर सात-आठ लाईनों की एक कविता लिखी कि इस बार अगर हरि ओम पंवार जी मिल गए तो उनको सुनाऊंगा परंतु बहुत दिनों तक, हरि ओम पँवार जी से मुलाकात नहीं हुई। फिर बाद में एक समारोह में आमना-सामना हुआ तो मैंने उनको चार लाईनें सुनाई। कविता लिखने का यह प्रयास निरंतर जारी रहा और धीरे-धीरे मैं कविता लिखने लगा। फिर विदेश से भी मुझे कविता पाठ के लिए निमंत्रण मिलने लगा और एक कवि के रूप में, मैं स्थापित हो गया। अतः यह कह सकता हूं कि प्रशासनिक सेवा में आने के बाद ही मैंने कविता लिखना पढ़ना शुरू किया। उर्दू का लहजा मैने अपने आसपास के वातावरण से ही सीखा।
 |
अशोक श्रीवास्तव ‘कुमुद’, डॉ. अखिलेश मिश्र, नरेश कुमार महरानी और डॉ. इम्तियाज़ अहमद ग़ाज़ी।
|
सवाल: प्रशासनिक पद पर रहते हुए, विभिन्न सामाजिक परिदृश्यों पर प्रायः खुलकर नहीं बोल पाने के कारण कवि हृदय अक्सर कसमसाहट और बेचैनी का अनुभव करता होगा, इस परिस्थिति से आप कैसे निपटते हैं?
जवाब: कोई भी बात कहने में, व्यक्तिगत रूप से मैं डरता नहीं था। कविता की अपनी एक विशेषता है कि कविता समझने वाले को ही चोट करती है। मेरी निर्भीकता तथा स्पष्टता पर, पहली बार जब पत्रकारों ने मुझसे कहा कि आप सुबह तक सस्पैंड हो जाओगे तब मैंने कहा कि अगर आप मेरे शब्दों को, घुमा-फिराकर लिखोगे तो सस्पैंड तो हो ही जाऊंगा, लेकिन सस्पैंड भी हो जाऊंगा तो क्यों हुआ, लोग जानेंगे तो कि ये कवि किस स्तर का है। मैं इस बात से कभी डरा नहीं और ये मेरा अनुभव है कि तमाम बड़े-बड़े दंगे जहां हो जाते हैं, वहां मेरे एक दो शेर ने वो काम कर दिया कि कोई दंगा नहीं हुआ। और मुझे याद है कि एक जगह मुस्लिम पापुलेशन बहुत अधिक थी। वहां पर लोगों ने कहा कि मियां अपने ख़्याल का आदमी है, शायरी करता है इसलिए अपने क्षेत्र में सब ठीक-ठाक रहना चाहिए और फिर कह देने मात्र से कोई बवाल नहीं करता था। इसी तरह हमारे हिंदू भाई भी होते थे, उनको मैं श्लोक वगैरह सुना दिया करता था तो भीड़ मेरे कंट्रोल में आ जाया करती थी। अगर यह नहीं होता तो गंभीर परिस्थितियों में, जितनी कठोरता, मुझे करनी पड़ी, उससे कहीं ज्यादा करनी पड़ती। मैं जिन क्षेत्रों में रहा हूं जैसे मेरठ, सहारनपुर, संभल आदि, ऐसे क्षेत्रों में पोस्टिंग होने की लिस्ट में मेरा नाम इसलिए ऊपर रहता था, कि जो बवाल होगा उसको मैं कुशलतापूर्वक निपटा लूंगा।
सवाल: आप विषम परिस्थितियों, जैसे दंगा कंट्रोल करते समय या चुनाव संचालन आदि के दौरान, आपका व्यक्तित्व जितना दृढ़संकल्प और कठोर नजर आता है। कवि के रूप में आपका हृदय उतना ही कोमल नज़र आता है। परिस्थितिजन्य या समय की मांग के अनुसार अपने अंदर यह सामंजस्य या बदलाव आप कैसे लाते हैं।
जवाब: मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि कलेक्टर चुनाव संचालन में वरिष्ठ अधिकारी होता है। वह सही समय पर, सही तरीके से, सही निर्णय कर दे तो कोई बवाल नहीं होता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। सही समय पर सही प्लानिंग के साथ आपकी निष्पक्षता बहुत मायने रखती है। चुनाव में हमारे पास पावर बहुत रहती है और आपका उद्देश्य मात्र एक है कि चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो जाय तो फिर अगर थोड़ी अशांति भी फैले तो कोई दिक्कत नहीं। आपका सर्वाेपरि उद्देश्य है, चुनाव संपन्न होना, तो चुनाव तो हो के रहेगा बाकी सारे विषय गौड़ हो जाते हैं। चुनाव होना है तो होना है। यूपी के हर कोने में चुनाव कराया है। एक-एक चीज़ नियमबद्ध है एक-एक लाइन लिखी हुई है। बहुत ज्यादा बुद्धी प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। नियमों और दिशा-निर्देशों पर क्लेयरिटी होनी चाहिए, फिर डरना किस बात का है।
सवाल: आपने देश विदेश में आयोजित अनेक कवि सम्मेलन या मुशायरों में मंच से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है, ऐसे किसी आयोजन के किसी खास संस्मरण के बारे में बताएं।
जवाब: मैं इमरान प्रतापगढ़ी के साथ हुए एक मुशायरे का जिक्र करना चाहूंगा। दुबई में एक प्रोग्राम हो रहा था उसमें हमारी शायरी और इमरान की शायरी में डिफ्रेंस था। मैं शायरी कर के गया और वो खड़ा हुआ। मेरी शायरी के बाद इमरान ने बोलना शुरू किया। बार बार अपनी शायरी में मेरा जिक्र किया कि इन्होंने यह कहा, इन्होंने ऐसा कहा और मैं यह कहना चाहता था। इमरान के फैन्स ने, जिन्होंने जब बार-बार मेरा नाम सुना तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर ढूंढ ढूंढ कर मेरा वीडियो बार बार देखा और सोशल मीडिया के द्वारा मेरे तथा मेरी शायरी के बारे में अच्छी तरह से जाना। तमाम लोग मुझसे मिलने आए। उनसे मैंने पूछा कि इतने लोग मुझे यहां कैसे जानते हैं तो उन्होंने बताया कि इमरान प्रतापगढ़ी ने आपका इतना अधिक जिक्र किया कि जिज्ञासावश लोगों ने सोशल मीडिया पर आपके वीडियो एवं रचनाएं ढूंढ-ढूंढ कर देखी, जिससे आप उनके जेहन मे बस गये। सऊदी जैसे देश में शायरी करना, बहुत मुश्किल काम है। अगर आपका एक लफ़़्ज़ गलत हो गया तो कोई भी कार्रवाई हो सकती है। यह मैं काफी पहले की बात बता रहा हूं। वहां काफी संभल के बोलना पड़ता है कि ऐसी कोई बात नहीं निकल जाय कि वहां की जो इंटलजेंसियां होती है वो आप पर कोई आरोप लगा दें।
सवाल: मंचीय मुशायरों पर हो रही चुटकले बाजी दोअर्थी शब्दों के प्रयोग पर आप का क्या दृष्टिकोण है ?
जवाब: हां, आप ठीक कह रहे हैं कि स्तर गिरता जा रहा है, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन आज का युग ऐसा हो गया है कि किसी को शुद्ध घी खिला देने से आदमी बीमार पड़ जाता है। थोड़ा सा नमक मिर्च तो चलता है परंतु कभी-कभी उसमें जो फूहड़पन आ जाता है वो गलत है। उसमें मंचीय कवि या शायर भले ही वो चुटकुलेवाला क्रियेटर है उसका अपना एक सम्मान होना चाहिए। उसको अपने सम्मान को एक सीमा से नीचे नहीं गिराना चाहिए। आर्गनाइजर को भी देखना चाहिए। अगर आप किसी भी कवि सम्मेलन के अर्थशास्त्र को देखें तो कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, जो कहते हैं कि आप अमुक कवि को बुलाओ तो हम फंड की व्यवस्था कर देंगे। अगर दो अर्थी शब्द भी ओरिजनल है, क्रिएटिव है आदमी का, उसे सुना सकता है, बाकी अभद्रता की भी एक सीमा होनी चाहिए। सीमा के बाहर अभद्रता नहीं। किसी की खूबसूरती की तारीफ ज़रूरत से ज्यादा, एक जो लकीर होती है उससे आगे बढ़कर, अगर आपने थोड़ा सा गलत शब्द इस्तेमाल कर किया तो अश्लील हो जाएगी।
सवाल: वर्तमान दौर में जबकि छंदमुक्त कविताओं ने हिंदी साहित्य में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है तब कविता की संरचना में छंदो की उपयोगिता पर आपका क्या विचार है ?
जवाब: छंद मुक्त कविता को मैं बहुत ज्यादा साहित्यिक नहीं मानता हूं। हालांकि छंदमुक्त में भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी गई हैं, एक से एक अच्छी कविता लिखी गई हैं जैसे निराला की कविता- वह आता--
दो टूक कलेजे को करता, पछताता
पथ पर आता।
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक,
चल रहा लकुटिया टेक’
निराला जी की यह कविता उच्चकोटि की साहित्यिक कविता है। अगर छंदमुक्त कविता बहुत उच्च कोटि की है तो चलेगी अन्यथा नहीं। मंच के सामने बैठे हुए आम श्रोताओं में से कुछ गीत समझते हैं, कुछ शायरी, गजल समझते हैं। छंदमुक्त कविता एकेडमिक दृष्टिकोण से तो ठीक है परंतु मंचीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाय तो अगर छंदमुक्त कविता में व्यक्तिगत परफार्मेंस बहुत ज्यादा रहेगी तो ही चलेगी। छंदीय कविता तो सब के अंदर होता है। बिना गेयता के कविता बन ही नहीं सकती। कवि मूलतः एक गीतकार ही होता है। गा सके या न गा सके यह अलग बात है।
सवाल: समाज में मानवीयता और सौहार्द बनाए रखने में कविता/ग़ज़ल का क्या किरदार हो सकता है ?
जवाब: बहुत बड़ा किरदार है और मैं एक लाइटर मोड में यह भी कहना चाहूंगा कि हम सब लोग यह कहते हैं कि गंगा-जमुनी सभ्यता होना चाहिए तो हम प्रयासरत रहते हैं कि सभ्यता के विरोधी अपना काम न कर जाएं। हृदय को स्पर्श करके, मन को स्पर्श करके, सच्चाई को बयान करके, यह सौहार्द बना रहे और बहुत ज्यादा मामलों में यह सौहार्द बना भी रहता है। इसका एक पहलू यह भी है कि जब हम शांति सभा की मीटिंग करते हैं, अलग अलग स्थितियों में, तो आप देखिए कि दो लाइन में कही गई बात, कितना असर डालती है। अब तो विधानसभा, लोक सभा और हर लोक पटल पर शायरी का अपना एक महत्व हो गया है। कविता डिलीवर तो करती है, कनेक्ट भी करती है। समाजिक सौहार्द में कविता का बहुत बड़ा रोल है।
सवाल: नौजवानों में हिंदी साहित्य के पठन-पाठन एवं सृजन के प्रति निरंतर घटते रुझान के संबंध में आपको क्या महसूस होता है ?
जवाब: बड़ी विडंबना है कि हमने हिंदी साहित्य को अर्थशास्त्र से नहीं जोड़ा। हम इसको अर्निंग (धनोपार्जन) का स्रोत नहीं बना सके। अभी हमने एक यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किया था कि आप इवेंट मैनेजमेंट में कविता, शायरी, गजल को प्रेजेंटेशन में शामिल करते हुए, मंच संचालन आदि पर एक प्रोजेक्ट बनाएं और अगर देखा जाए तो इसमें बहुत अर्निंग स्कोप भी है। अगर हम किसी तरह से हिंदी साहित्य को अर्थशास्त्र (धनोपार्जन) से जोड़ दें, तो इसकी उपयोगिता स्वतः बढ़ जायेगी। हम खेल में एक अच्छे खिलाड़ी को रिजर्वेशन देते हैं परंतु एक साहित्यकार को नहीं। क्रिएटर (रचनाकार) को नहीं देते। अभी इस पर हम धीरे-धीरे जागरूक हो रहे हैं। जितने भी हमारे वेद, पुराण, पुरानी पुस्तकें हैं जिन पर आज विदेशों में रिसर्च चल रही है, उसको पढ़ाने के लिए ही अलग से व्यवस्था की जा रही है। चरक को पढ़ लीजिए तो बड़े बड़े डाक्टर फेल हो जाएं। साहित्य मे जो बात कह दी गई हैं वहां तक हमारा विज्ञान, आज की भाषाएं पहुंच नहीं सकती। फिर कमी कहां रह गई कि अभी भी हम इसको अर्थ से नहीं जोड़ पाए। जिस दिन साहित्य, अर्थ से जुड़ना शुरू होगा, लोग साहित्य पढ़ना शुरू करेंगे और इसके लिए कुछ करना पड़ेगा इसके लिए मौलिक सोच एवं कार्य चाहिए।
(गुफ़्तगू के अक्तूबर-2023 अंक में प्रकाशित)